Aacharya Hajari Prasad dwivedi jivan parichay-हजारी प्रसाद द्विवेदी
हेल्लो दोस्तों, आज मैं आपको Aacharya Hajari Prasad dwivedi jivan parichay के बारे में बताऊंगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक लेखक, साहित्यकार एवं इतिहास विशेषज्ञ थे। हिन्दी लेखन में द्विवेदी जी के वृत्तान्तों का एक विशिष्ट व्यक्तित्व है। वे अनेक बोलियों में पारंगत थे। हिंदी के अलावा, उन्हें संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश बोलियों की व्यापक समझ थी।
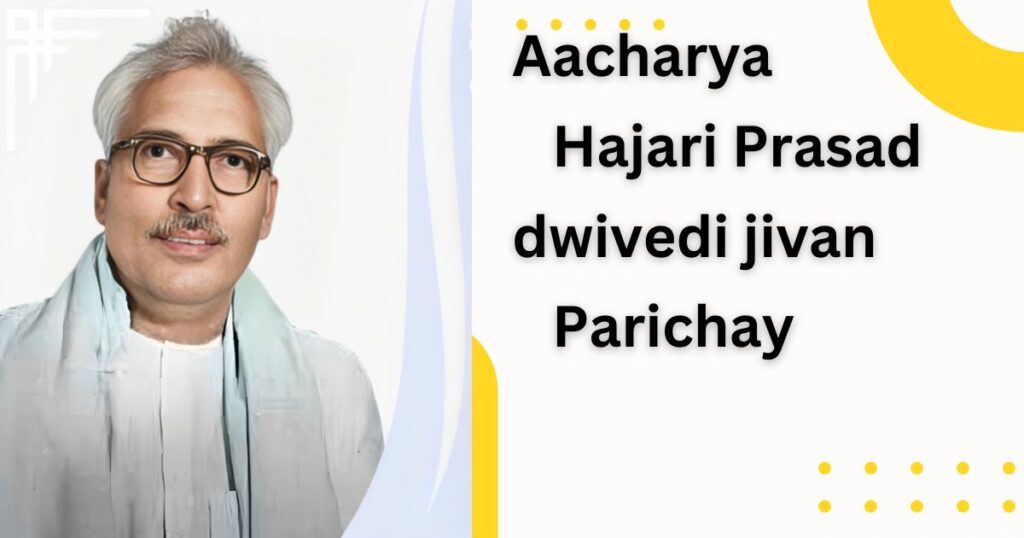
हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय
हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक और भारतीय संस्कृति के समसामयिक व्याख्याता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ई. में बलिया जिले के ‘दूबे का छपरा’ नामक गाँव में हुआ था। उन्हें संस्कृत और ज्योतिष का ज्ञान अपने पिता पंडित अनमोल दुबे से विरासत में मिला था। 1930 ई. में उन्होंने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से ज्योतिषी की उपाधि प्राप्त की। 1940 से 1950 ई. तक वे शान्ति निकेतन में हिन्दी भवन के निदेशक पद पर कार्यरत रहे। व्यापक स्वाध्याय एवं साहित्य सृजन की आधारशिला यहीं रखी गयी।
1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। 1950 ई. में वे बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष बने तथा 1960 से 1966 तक वे पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। 1957 ई. में उन्हें ‘पद्मभूषण’ की उपाधि से सम्मानित किया गया। अनेक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हुए उन्होंने 1979 में रोगशय्या पर चिर निद्रा ले ली अर्थात उनका निधन हो गया।
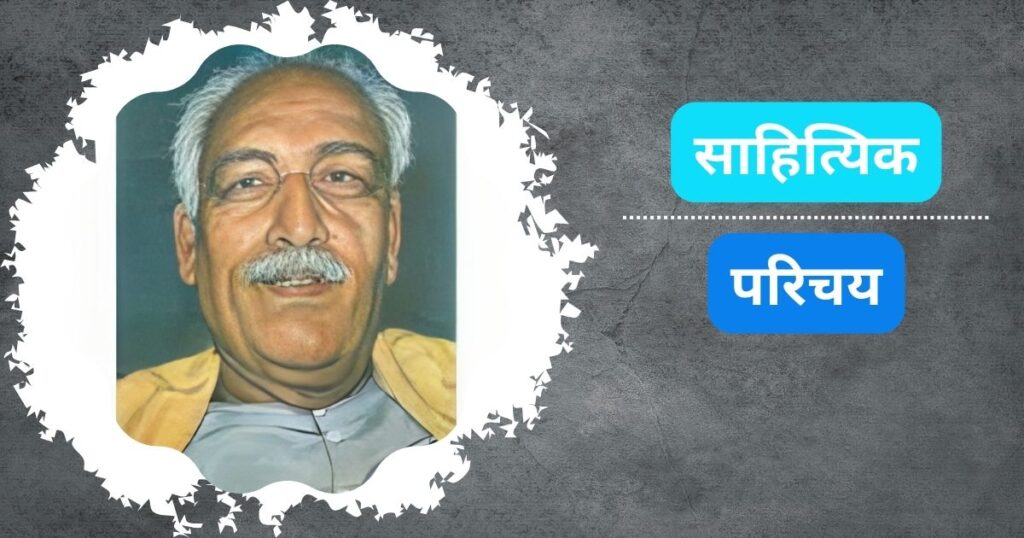
Aacharya hajari prasad dwivedi ka sahityik parichay-साहित्यिक-परिचय
आधुनिक युग के गद्य लेखकों में आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। हिन्दी गद्य के क्षेत्र में उनका साहित्यिक परिचय इस प्रकार दिया जा सकता है-
1. निबन्धकार के रूप में – आचार्य द्विवेदी के निबंधों में जहां साहित्य और संस्कृति की अविरल धारा प्रवाहित होती है, वहीं दैनिक जीवन की विभिन्न गतिविधियों, क्रियाकलापों, अनुभवों आदि का चित्रण भी बड़ी सजीवता और मार्मिकता के साथ किया गया है।
2. आलोचक के रूप में – आलोचनात्मक साहित्य सृजन की दृष्टि से द्विवेदीजी का महत्वपूर्ण स्थान है। उनके आलोचनात्मक कार्यों में विद्वता एवं पांडित्य स्पष्ट दिखाई देता है। ‘सूर-साहित्य’ उनकी प्रारंभिक आलोचनात्मक कृति है। इसमें भावुकता अधिक है। इसके अलावा उनके कई मार्मिक एवं आलोचनात्मक निबंध विभिन्न निबंध संग्रहों में संग्रहित हैं।
3. उपन्यासकार के रूप में – द्विवेदीजी ने चार महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे हैं। ये हैं- ‘बाणभट्ट की आत्मकथा’, ‘चारु-चन्द्र-लेख’, ‘पुनर्नवा’ और ‘अनामदास का पोथा’। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित ये उपन्यास द्विवेदी जी की गंभीर चिंतन शक्ति का प्रमाण हैं। इतिहास और कल्पना को मिलाकर लेखक ने अपने उपन्यास-साहित्य को आकर्षक रूप दिया है।
4. ललित निबंधकार के रूप में द्विवेदी जी ने ललित निबंध के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण लेखन कार्य किया है। हिन्दी के ललित निबंधों को व्यवस्थित रूप देने वाले निबंधकार के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद अग्रणी हैं। द्विवेदीजी के ललित निबंधों में रसास्वादन की अद्वितीय क्षमता है। भावुकता, कामुकता एवं कोमलता के साथ-साथ आवेगपूर्ण प्रतिपादन की शैली भी है। निश्चय ही वे ललित निबंध के क्षेत्र में अग्रणी लेखक रहे हैं।
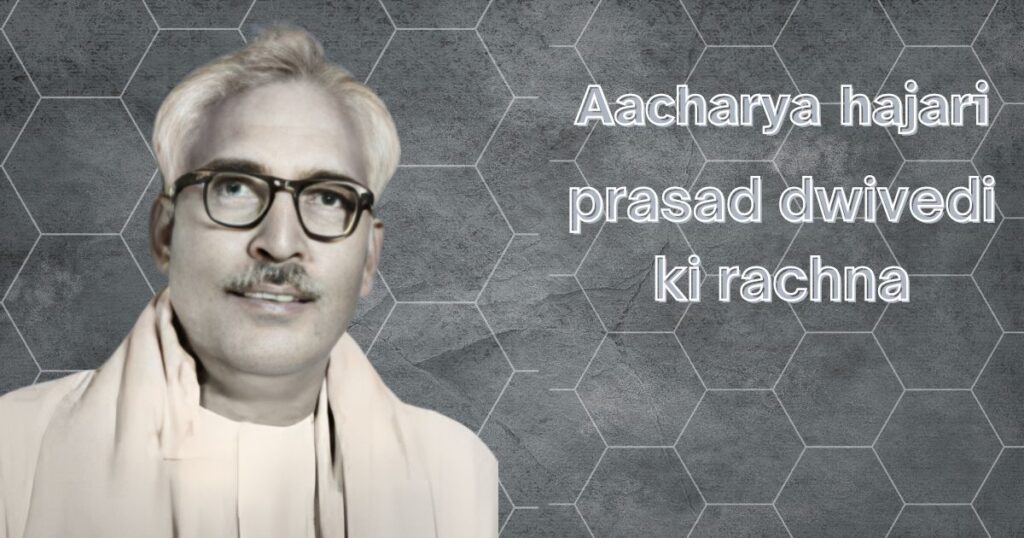
Aacharya hajari prasad dwivedi ki rachna-कृतियाँ
आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने अनेक पुस्तकों की रचना की, जो निम्नलिखित खण्डों में प्रस्तुत हैं-
- निबन्ध संग्रह – (1) अशोक के फूल, (2) कुटज, (3) विचार प्रवाह, (4) विचार और वितर्क, (5) आलोक पर्व, (6) कल्पलता।
- आलोचना – साहित्य – (1) सूर – साहित्य, (2) कालिदास की लालित्य योजना, (3) कबीर, (4) साहित्य – सहचर, (5) साहित्य का मर्म।
- इतिहास – (1) हिन्दी साहित्य की भूमिका, (2) हिन्दी – साहित्य का आदिकाल, (3) हिन्दी साहित्य।
- उपन्यास – (1) बाणभट्ट की आत्मकथा, (2) चारु चन्द्र-लेख, (3) पुनर्नवा, (4) अनामदास का पोथा।
- सम्पादन – (1) नाथ – सिद्धों की बानियाँ, (2) संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, (3) सन्देश – रासक।
- अनूदित रचनाएँ – (1) प्रबन्ध – चिन्तामणि, (2) पुरातन – प्रबन्ध-संग्रह, (3) प्रबन्ध-कोश, (4) विश्व परिचय, (5) लाल कनेर, (6) मेरा बचपन आदि। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने अनेक पुस्तकों की रचना की, जो निम्नलिखित खण्डों में प्रस्तुत हैं-
भाषा-शैली
भाषा – द्विवेदी जी सहज भाव से अपने विचार व्यक्त करते थे। उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया जो कृत्रिम या प्रयासपूर्ण हो। उनकी भाषा पर बोलचाल की भाषा हावी हो गई है। उन्होंने सभी प्रचलित भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करके हिंदी को समृद्ध तो किया, परंतु ऐसी शब्दावली का प्रयोग उन्होंने हिंदी की प्रकृति के अनुकूल बनाकर ही किया।
द्विवेदीजी ने संस्कृत शब्दावली को अधिकतर तत्सम रूप में ही स्वीकार किया है; जैसे- भण्डार, भग्नावशेष, प्रारंभ, क्रियमाण, उत्सुक्य, सलज्ज, अवगुंठन आदि।
भाषा को लोकप्रिय, सरस एवं मनोरंजक बनाने तथा अपने मत के समर्थन के लिए संस्कृत, हिन्दी, बाँग्ला आदि की सूक्तियों का भी पर्याप्त प्रयोग किया है।
मुहावरों और लोकोक्तियों को उन्होंने स्थानीय बोलचाल की भाषा से ग्रहण किया है।
शैली – आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने विभिन्न विषयों पर आधारित निबंधों की रचना की है। उनके निबंध अनेक शैलियों में लिखे गये हैं। द्विवेदीजी की शैलीगत विशेषताएँ मुख्यतः इस प्रकार हैं-
1. गवेषणात्मकता ( गवेषणात्मक शैली) – द्विवेदीजी ने शोध एवं पुरातत्व संबंधी निबंध गवेषणात्मक शैली में लिखे हैं। इस शैली पर आधारित निबंध साहित्यिक गरिमा से परिपूर्ण है। साहित्य के विभिन्न पहलुओं पर विचार करते समय और शब्दों के नाम, संरक्षक और सुप्रसिद्धि का पता लगाते समय आचार्य द्विवेदी की खोजी प्रतिभा विशेष रूप से दृष्टिगोचर होती है।
2. वैयक्तिकता ( आत्मपरक शैली) – गम्भीर स्थानों पर जब सन्दर्भ में घनिष्ठता उत्पन्न हो गई हो अथवा जब द्विवेदी जी स्वयं को सन्दर्भ से जोड़ना चाहते हों, तब उनकी शैली व्यक्तिपरक हो गई है। इस शैली में सहजता, दयालुता और काव्यात्मकता के गुण विद्यमान हैं।
3. विचारात्मकता (विचारात्मक शैली) – द्विवेदीजी के अधिकांश निबंध विचारपूर्ण हैं। चिंतनशील शैली साहित्यिक, धार्मिक और सांस्कृतिक निबंधों में विशेष रूप से सफल साबित हुई है। उन्होंने गंभीर से गंभीर विषय को भी बड़ी कुशलता और बोधगम्यता से प्रस्तुत किया है।
4. वर्णनात्मकता (वर्णनात्मक शैली) – द्विवेदीजी विषय को रोचक बनाने में पक्षपाती हैं, इसीलिए उन्होंने कहीं-कहीं वर्णनात्मकता का सहारा लिया है। उनकी वर्णनात्मक शैली इतनी सजीव है कि वह एक चित्र प्रस्तुत करती है।
5. आलंकारिकता (आलंकारिक शैली) – अभिव्यक्ति को चमत्कार प्रदान करने के लिए द्विवेदीजी ने कहीं-कहीं आलंकारिक शैली का भी प्रयोग किया है। इस शैली के प्रयोग से उनका गद्य काव्य के समान मनोरम हो गया है।
6. व्यंग्यात्मकता ( व्यंग्यात्मक शैली) – इस शैली के अन्तर्गत द्विवेदीजी ने बड़ी मीठी चुटकियाँ ली हैं। साहित्यकारों और प्रचलित साहित्यिक प्रवृत्तियों पर इन्होंने करारे व्यंग्य किए हैं
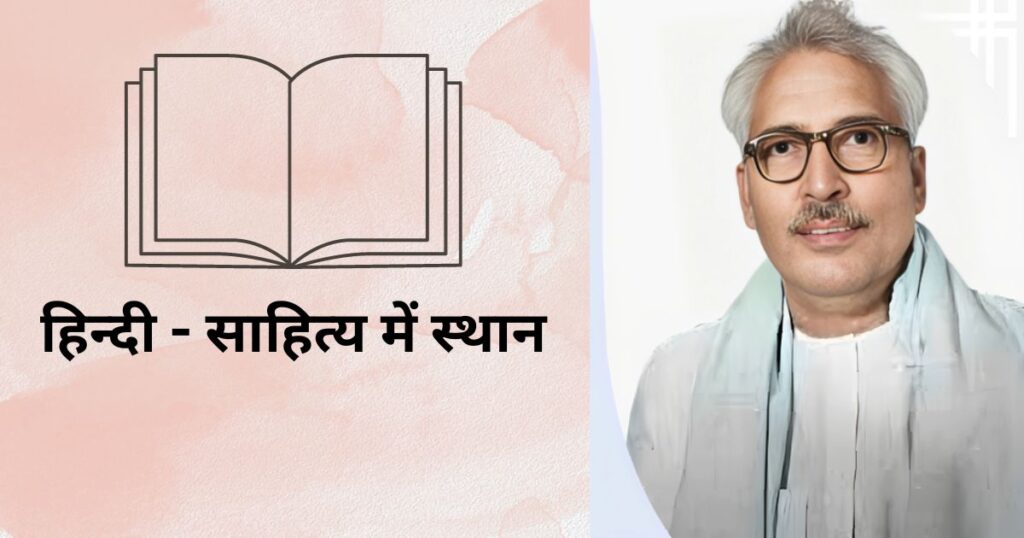
हिन्दी – साहित्य में स्थान
डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएँ हिन्दी साहित्य की अमूल्य निधि हैं। उनके निबंधों और आलोचनाओं में उच्च स्तरीय चिंतन क्षमता दृष्टिगोचर होती है। हिंदी साहित्य जगत में वे एक विद्वान आलोचक, निबंधकार और आत्मकथा लेखक के रूप में विख्यात हैं। उनके कल्पनाशील निबंध हिंदी में बेजोड़ हैं और उनकी साहित्यिक सेवा अद्वितीय है। हिन्दी आलोचकों में उनका स्थान महत्त्वपूर्ण है।
FaQ’s
डॉ हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी आलोचना के क्षेत्र में क्या योगदान है?
उन्होंने मूलतः हिन्दी साहित्य के परिचय में आलोचना की ऐतिहासिक तकनीक का परिचय दिया। 2) हजारी प्रसाद द्विवेदी के आधुनिकतावादी दृष्टिकोण ने कबीर के अद्यतन मूल्यांकन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कबीर को सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और साहित्यिक निरंतरता के व्यापक दृष्टिकोण से देखने का प्रभावी प्रयास किया।
हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य कौन थे?
उनके प्रिय शिष्य प्रो. विश्वनाथ त्रिपाठी ने द्विवेदी जी के जीवन और रचनात्मक जगत पर ‘व्योमकेश दरवेश (आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी स्मृति)’ नाम से एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है। ऐसी ही एक किताब उनके दूसरे शिष्य नामवर सिंह ने भी लिखी है जिसका शीर्षक है ‘दूसरी परंपरा की खोज’.
हिंदी की पहली पुस्तक कौन सी है?
पृथ्वीराज रासो की पुस्तक को हिंदी का पहला प्रकाशन माना जाता है। पृथ्वीराज रासो नामक ब्रजभाषा महाकाव्य 12वीं शताब्दी के भारतीय राजा पृथ्वीराज चौहान की कहानी कहता है। यह उपलब्धि चंदबरदाई की है।

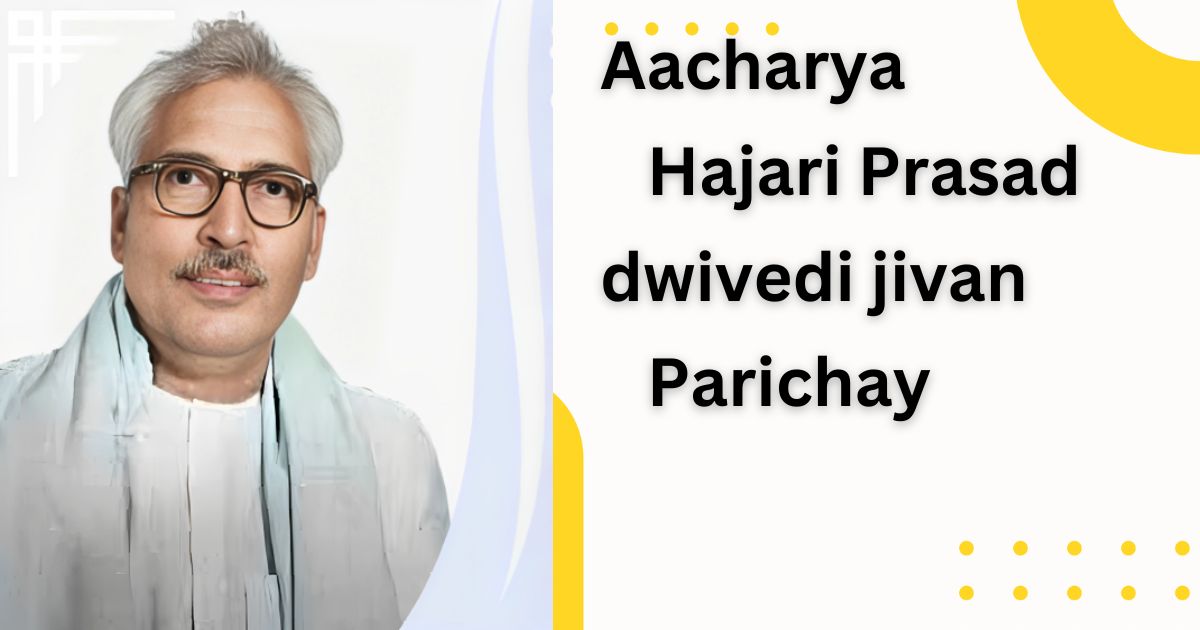

1 thought on “Aacharya Hajari Prasad dwivedi jivan parichay-हजारी प्रसाद द्विवेदी”